“नाथ संप्रदाय” नामक पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक ऐसी कालजयी कृति है, जिसमें उन्होंने गोरखनाथ और उनके संप्रदाय को न केवल धार्मिक या आध्यात्मिक संदर्भ में, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, और साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी विद्वता और संवेदनशीलता के साथ इस संप्रदाय की ऐसी गहन पड़ताल की, जिससे यह पुस्तक भारतीय दर्शन और साहित्य के अध्येताओं के लिए अमूल्य बन गई।
गोरखनाथ को एक योगी, समाज सुधारक, और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में चित्रित करते हुए द्विवेदी जी ने दिखाया कि नाथ संप्रदाय ने मध्यकालीन भारत में योग, तंत्र, और भक्ति के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। सन् 1950 में प्रकाशित इस पुस्तक की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, क्योंकि यह योग की वैश्विक लोकप्रियता और भारतीय आध्यात्मिकता के ऐतिहासिक विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पुस्तक के मुताबिक, नाथ संप्रदाय न केवल एक आध्यात्मिक आंदोलन है, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकीकरण का सार्थक प्रयास भी है।
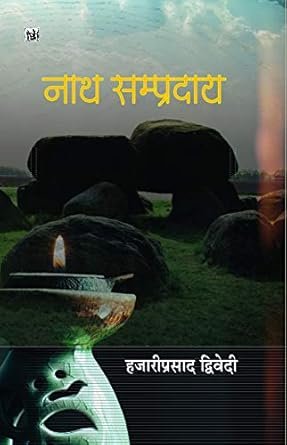 पुस्तक में उल्लेख है कि नाथ संप्रदाय की जड़ें प्राचीन शैव परंपराओं और तांत्रिक साधनाओं में निहित हैं। इसका प्रतीकात्मक संस्थापक आदिनाथ (भगवान शिव) को माना जाता है, जिन्हें प्रथम गुरु के रूप में पूजा जाता है। मानव गुरुओं में मत्स्येंद्रनाथ (मीननाथ) को संप्रदाय का प्रथम ऐतिहासिक गुरु माना गया, जिन्होंने तंत्र और योग के सिद्धांतों को व्यवस्थित किया। उनके शिष्य गोरखनाथ ने इस परंपरा को संगठित और लोकप्रिय बनाया। पुस्तक में नाथ संप्रदाय के ऐतिहासिक विकास को 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच रखा गया है, हालाँकि सटीक तिथियाँ किंवदंतियों और परंपराओं के कारण अस्पष्ट हैं। द्विवेदी जी ने मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की कथाओं को ऐतिहासिक तथ्यों और प्रतीकात्मक व्याख्याओं के साथ जोड़ा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये योगी केवल साधक नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन के ध्वजवाहक भी थे।
पुस्तक में उल्लेख है कि नाथ संप्रदाय की जड़ें प्राचीन शैव परंपराओं और तांत्रिक साधनाओं में निहित हैं। इसका प्रतीकात्मक संस्थापक आदिनाथ (भगवान शिव) को माना जाता है, जिन्हें प्रथम गुरु के रूप में पूजा जाता है। मानव गुरुओं में मत्स्येंद्रनाथ (मीननाथ) को संप्रदाय का प्रथम ऐतिहासिक गुरु माना गया, जिन्होंने तंत्र और योग के सिद्धांतों को व्यवस्थित किया। उनके शिष्य गोरखनाथ ने इस परंपरा को संगठित और लोकप्रिय बनाया। पुस्तक में नाथ संप्रदाय के ऐतिहासिक विकास को 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच रखा गया है, हालाँकि सटीक तिथियाँ किंवदंतियों और परंपराओं के कारण अस्पष्ट हैं। द्विवेदी जी ने मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की कथाओं को ऐतिहासिक तथ्यों और प्रतीकात्मक व्याख्याओं के साथ जोड़ा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये योगी केवल साधक नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन के ध्वजवाहक भी थे।
यह पुस्तक गोरखनाथ के जीवन, उनकी शिक्षाओं, और योगदान पर केंद्रित है। द्विवेदी जी गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व मानते हैं, जिन्होंने हठयोग को एक व्यवस्थित रूप दिया और तंत्र को जनसामान्य तक पहुँचाया। गोरखनाथ को एक ऐतिहासिक योगी के साथ-साथ लोककथाओं और किंवदंतियों का नायक भी बताया गया है। उनकी जीवनी में चमत्कारों और सिद्धियों की कथाएँ प्रचलित हैं, जिन्हें द्विवेदी जी प्रतीकात्मक रूप से उनकी आध्यात्मिक शक्ति और प्रभाव के रूप में व्याख्यायित किया। गोरखनाथ की शिक्षाओं में हठयोग यथा आसन, प्राणायाम, और मुद्राओं के साथ-साथ कुंडलिनी योग और आत्म-साक्षात्कार पर भी बल दिया गया। द्विवेदी जी बताते हैं कि गोरखनाथ ने तंत्र की जटिल और रहस्यमयी प्रथाओं को सरल बनाकर योग और ध्यान के साथ जोड़ा, जिससे यह साधना आम लोगों के लिए सुलभ हो सकी। उनकी वाणियाँ, जैसे “गोरक्ष शतक” और “सबदी”, सरल भाषा में गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार व्यक्त करती हैं। इनमें सत्य, संयम, और गुरु-भक्ति के साथ-साथ माया और आत्मा के रहस्यों का वर्णन है।
पुस्तक में नाथ संप्रदाय के दर्शन को अद्वैत वेदांत, शैव तंत्र, और योग के समन्वय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका मूल लक्ष्य आत्मा का परमात्मा से मिलन और मोक्ष की प्राप्ति है। नाथ दर्शन की प्रमुख विशेषताओं में हठयोग, कुंडलिनी योग, गुरु-शिष्य परंपरा और निर्गुण भक्ति का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। द्विवेदी जी ने इस दर्शन को मध्यकालीन भारत की धार्मिक गतिशीलता के संदर्भ में रखा, जहाँ यह वैदिक कर्मकांडों और बौद्ध तंत्र के बीच एक संतुलन स्थापित करता था।
द्विवेदी जी ने नाथ संप्रदाय के सामाजिक योगदान को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए लिखा कि यह संप्रदाय जाति, वर्ग, और लिंग भेद से ऊपर उठकर सभी को साधना का अधिकार देता था। गोरखनाथ और अन्य नाथ योगियों ने समाज के निचले वर्गों को आध्यात्मिक मार्ग प्रदान किया, जिससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिला। उनकी सादगी और साहस ने उन्हें जनमानस में लोकप्रिय बनाया। पुस्तक में यह भी बताया गया कि नाथ संप्रदाय ने हिंदी साहित्य और भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। गोरखनाथ की वाणियाँ और अन्य नाथ साहित्य ने हिंदी की अवधी और ब्रज भाषाओं को समृद्ध किया। कबीर, नानक, और अन्य निर्गुण भक्ति संतों पर नाथ विचारों का प्रभाव स्पष्ट है। द्विवेदी जी ने इसे एक सांस्कृतिक पुल के रूप में देखा, जो वैदिक और लोक परंपराओं को जोड़ता था।
नाथ संप्रदाय के साहित्यिक योगदान पर चर्चा करते हुए द्विवेदी जी ने गोरखनाथ और उनके अनुयायियों की रचनाओं का विश्लेषण किया। “गोरक्ष शतक”, “सिद्ध सिद्धांत पद्धति”, और “योग बीज” जैसे ग्रंथों में योग और तंत्र के सिद्धांतों को व्यवस्थित किया गया। गोरखनाथ की वाणियाँ सरल और काव्यात्मक थीं, जो आम जन तक आध्यात्मिक संदेश पहुँचाती थीं। उदाहरण के लिए, उनकी एक वाणी है: “सबदे मरै सो जीवै सदा, जो मरि जीवै सोई सिद्ध सारा।” इसका अर्थ है कि जो अहंकार को मिटाकर शब्द (आत्म-ज्ञान) में लीन होता है, वही सदा जीवित रहता है। द्विवेदी जी ने इन रचनाओं को हिंदी साहित्य की प्रारंभिक कृतियों के रूप में देखा, जो मध्यकालीन भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। साथ ही नाथ साहित्य को भक्ति और योग के बीच सेतु के रूप में रेखांकित किया।
पुस्तक में नाथ संप्रदाय के भौगोलिक और सांस्कृतिक प्रसार का वर्णन है, जो उत्तर भारत (पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान), पश्चिमी भारत (गुजरात, महाराष्ट्र), और पूर्वी भारत (बंगाल, असम) में फैला है। नेपाल में भी इसका गहरा प्रभाव रहा है। गोरखनाथ मंदिर (गोरखपुर) और अन्य नाथ मठ आज भी इस परंपरा के केंद्र हैं। द्विवेदी जी ने नाथ संप्रदाय की सीमाओं और आलोचनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने स्वीकार किया कि समय के साथ संप्रदाय में कुछ रूढ़ियाँ और अंधविश्वास प्रवेश कर गए, जिससे इसका मूल दर्शन धूमिल हुआ। फिर भी, उन्होंने इसके योग और तंत्र के योगदान को अपरिहार्य माना। उनकी लेखनी में तटस्थता और विद्वत्तापूर्ण दृष्टिकोण झलकता है, जो ऐतिहासिक तथ्यों और प्रतीकात्मक व्याख्याओं के बीच संतुलन बनाए रखता है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व अध्यात्म विज्ञान विश्लेषक हैं।)




