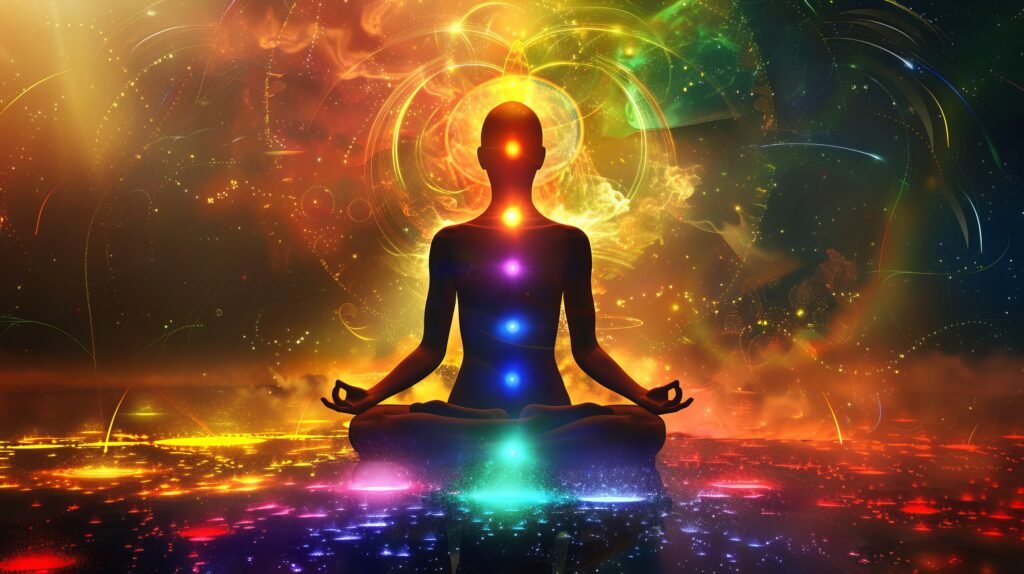हम अक्सर सोचते हैं कि योग मतलब सिर्फ आसन और प्राणायाम। लेकिन योग इससे कहीं ज्यादा है। योग का असली मतलब है—शरीर, मन और भावनाओं में तालमेल। यानी, सामंजस्य। अगर शरीर बीमार है, तो उसे ठीक करना होगा। अगर मन अशांत है, तो उसे शांत करना होगा। बिना सामंजस्य के जीवन अधूरा है।
हम योग शुरू करते हैं शरीर से। क्यों? क्योंकि शरीर को हम सबसे बेहतर समझते हैं। दर्द हो, जकड़न हो, या बीमारी—हमें तुरंत पता चलता है। इसलिए, आसन, प्राणायाम और हठ योग के अभ्यास से हम शरीर को संतुलित करते हैं। जब शरीर ठीक होता है, तो मन की बारी आती है। हम महसूस करते हैं—तनाव है, दबाव है। योग हमें सिखाता है—तनाव कैसे कम करें, मन कैसे शांत करें, और खुद को कैसे केंद्रित करें। इस तरह, योग हमें शरीर से मन की ओर ले जाता है। लेकिन योग यहीं नहीं रुकता। यह हमें आध्यात्मिक स्तर तक ले जा सकता है। पर हम अक्सर मन की थोड़ी-सी शांति पाकर रुक जाते हैं। सोचते हैं, बस, हो गया। लेकिन जीवन के और भी आयाम हैं। हमें उन्हें समझना होगा।
योग कहता है, इंसान का व्यक्तित्व बहुत विशाल है। यह सिर्फ इच्छाओं या आकांक्षाओं तक सीमित नहीं। योग का लक्ष्य है हमारी पूरी शख्सियत को निखारना। हम भौतिक से लेकर आध्यात्मिक स्तर तक जीते हैं। इन सभी स्तरों को समझकर ही हम योग का सही उपयोग कर सकते हैं।
योग का अंतिम लक्ष्य है—जीवन में पूर्णता। और यह पूर्णता आती है खुद को जानने से। लेकिन खुद को जानना क्या है? सोचिए—हम दूसरों को तो समझने का दावा करते हैं, पर खुद को कितना जानते हैं? बिना वजह क्यों कभी खुश, कभी दुखी हो जाते हैं? क्यों कभी प्यार बरसाते हैं, तो कभी गुस्से से जलने लगते हैं? जो खुद को नहीं जानता, वह दूसरों को क्या जानेगा?
योग जीवन को बदल देता है। लेकिन आसन और प्राणायाम को ही योग न समझें। ये योग के सिर्फ दो अंग हैं, पूरा योग नहीं। योग है—खुद को जानने की कला, सामंजस्य की कला। तो आइए, आज खुद से सवाल करें – मैं कौन हूं? तमिलनाडु का छात्र वेंकटरमण अय्यर खुद से यही सवाल पूछ-पूछ कर ज्ञानयोगी बन गया था, जिसे आज हम रमण महर्षि के नाम से जानते हैं। वे बीसवीं सदी के महान संत थे। उनका समाधि दिवस बीते 14 अप्रैल को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया।