वैदिक परंपरा में गुरु को वह प्रकाश माना गया है, जो शिष्य के जीवन से अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है। चाहे वह आदियोगी शिव हों, ऋषि वशिष्ठ हों, भगवान श्रीकृष्ण हों, आद्यगुरू शंकराचार्य हों, या द्रोणाचार्य, सभी ने अपने शिष्यों को न केवल ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें जीवन के उच्च आदर्शों, धर्म, और कर्तव्य के प्रति जागरूक किया। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन गुरु के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और श्रद्धा प्रकट करने का अवसर है। अच्छी बात यह है कि यह परंपरा आधुनिक युग में किसी न किसी रूप में मौजूद है।
 गुरू की महत्ता क्यों है, इसे रामायणकालीन कथा से समझा जा सकता है। चित्रकूट स्थित मंदाकिनी नदी का तट प्राचीन काल से ही ऋषि अत्रि, अनुसूया, भारद्वाज जैसे महान तपस्वियों की साधना-स्थली रहा है। इस पवित्र तट पर ही रामभक्त संत तुलसीदास अपने अश्रुपूरित नेत्रों से चंदन घिस रहे थे। उनकी भक्ति और विरह की गहराई उनके आंसुओं में झलक रही थी। तभी, भगवान श्रीराम और लक्ष्मण बालक रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, “बाबा, थोड़ा चंदन दे दो।” भक्ति में लीन तुलसीदास ने बिना बालकों की ओर देखे उत्तर दिया, “बच्चा, हमें क्यों परेशान करते हो? घाट पर और लोग भी हैं, उनसे ले लो। मुझे क्यों तंग करते हो बच्चा? मैं तो वैसे ही बहुत परेशान हूं।”
गुरू की महत्ता क्यों है, इसे रामायणकालीन कथा से समझा जा सकता है। चित्रकूट स्थित मंदाकिनी नदी का तट प्राचीन काल से ही ऋषि अत्रि, अनुसूया, भारद्वाज जैसे महान तपस्वियों की साधना-स्थली रहा है। इस पवित्र तट पर ही रामभक्त संत तुलसीदास अपने अश्रुपूरित नेत्रों से चंदन घिस रहे थे। उनकी भक्ति और विरह की गहराई उनके आंसुओं में झलक रही थी। तभी, भगवान श्रीराम और लक्ष्मण बालक रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, “बाबा, थोड़ा चंदन दे दो।” भक्ति में लीन तुलसीदास ने बिना बालकों की ओर देखे उत्तर दिया, “बच्चा, हमें क्यों परेशान करते हो? घाट पर और लोग भी हैं, उनसे ले लो। मुझे क्यों तंग करते हो बच्चा? मैं तो वैसे ही बहुत परेशान हूं।”
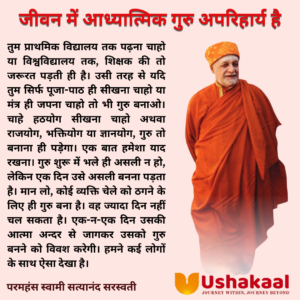 भगवान श्रीराम तो अपने प्रिय भक्त पर कृपा बरसाने के लिए लीला कर रहे थे। उन्होंने कहा, “अच्छा बाबा, चंदन न सही, पर यह तो बता दो, तुम रो क्यों रहे हो?” परेशान हाल संत तुलसीदास ने उत्तर दिया, “बच्चा, मेरे भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे।” राम जी ने कहा, “तब तो तुम्हारे भगवान बड़े कठोर हैं। इतनी गहन भक्ति के बाद भी दर्शन नहीं दे रहे!” यह सुनते ही तुलसीदास जी खड़े हुए और बालक के मुख पर हाथ रखकर कहा, “ऐसा मत कहो बच्चा! मेरे भगवान अत्यंत कृपालु और दयालु हैं। कमी तो मुझ में ही है, जिसके कारण मुझे उनके दर्शन नहीं हो रहे।” उसी क्षण, हनुमान जी तोते के रूप में प्रकट हुए। संत तुलसीदास जी ने लिखा है, “श्री रघुवीर खड़े हैं सनमुख, तुलसी तू क्यों रोता। सफल करो दृग, हनुमान जी बोले बन कर तोता।।” तुलसीदास जी की आँखें खुलीं, और उन्होंने अपने प्रिय राम के दर्शन किए।
भगवान श्रीराम तो अपने प्रिय भक्त पर कृपा बरसाने के लिए लीला कर रहे थे। उन्होंने कहा, “अच्छा बाबा, चंदन न सही, पर यह तो बता दो, तुम रो क्यों रहे हो?” परेशान हाल संत तुलसीदास ने उत्तर दिया, “बच्चा, मेरे भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे।” राम जी ने कहा, “तब तो तुम्हारे भगवान बड़े कठोर हैं। इतनी गहन भक्ति के बाद भी दर्शन नहीं दे रहे!” यह सुनते ही तुलसीदास जी खड़े हुए और बालक के मुख पर हाथ रखकर कहा, “ऐसा मत कहो बच्चा! मेरे भगवान अत्यंत कृपालु और दयालु हैं। कमी तो मुझ में ही है, जिसके कारण मुझे उनके दर्शन नहीं हो रहे।” उसी क्षण, हनुमान जी तोते के रूप में प्रकट हुए। संत तुलसीदास जी ने लिखा है, “श्री रघुवीर खड़े हैं सनमुख, तुलसी तू क्यों रोता। सफल करो दृग, हनुमान जी बोले बन कर तोता।।” तुलसीदास जी की आँखें खुलीं, और उन्होंने अपने प्रिय राम के दर्शन किए।
तब, संत तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी को गुरू माना और उनकी स्तुति में हनुमान चालीसा कुछ इस तरह शुरू किया, “श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। वरनऊँ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चारि॥“ संत राजेश्वरानंद सरस्वती कहते थे कि जो मिले मिलाए भगवान से परिचय करा दे, वही गुरू है। भगवान तो सभी के हृदय में विराजमान हैं। श्रीमद्भगवत गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, “ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।” यानी, ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यन्त्र पर आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियों को (उनके स्वभाव के अनुसार) भ्रमण कराता रहता है। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं कि प्रभु सबके हृदय में अछूते और अविकारी रूप में बसे हैं। फिर भी, मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाता। गुरुदेव का कार्य उस मिले हुए को पहचानने की दृष्टि देना है। मंदाकिनी के तट पर भी तो भगवान संत तुलसीदास के सम्मुख खड़े थे। पर, तुलसीदास जी पहचान नहीं पा रहे थे। श्री हनुमानजी बीच में आए तो भक्त और भगवान का मिलन हो गया। इसलिए तो संत कबीर कहते हैं, “गुरू गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पांय। बलिहारी गुरू अपने गोविन्द दियो बताय।।” दरअसल, वे गुरु के चरण चुनते हैं, क्योंकि गुरु ने असंभव को संभव बनाया और परमात्मा की दूरस्थ रोशनी को शिष्य तक पहुंचाया। गुरु के पास कुछ भी अपना नहीं; वह शून्यवत है, केवल परमात्मा का प्रतिबिंब है।
वैसे तो गुरु पूर्णिमा का पर्व वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वेदव्यास ने ही वेदों का संकलन किया और महाभारत की रचना की। उनकी शिक्षाएँ आज भी प्रासंगिक हैं। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रतीक है। पर, ओशो का दृष्टिकोण थोड़ा भिन्न है। वे कहते हैं कि शरद पूर्णिमा जैसी सुंदर तिथि की उपलब्धता के बावजूद आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में चुनाव के पीछे बड़ा आध्यात्मिक कारण रहा होगा। शरद पूर्णिमा में आकाश साफ होता है, चांद स्पष्ट दिखता है, पर यह केवल गुरु की सुंदरता को दर्शाता। आषाढ़ में बादल छाए रहते हैं, चांद की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुंचती। यह शिष्य के मन की स्थिति का प्रतीक है। शिष्य का मन अंधेरा, कामनाओं और जन्मों-जन्मों के संस्कारों से बोझिल होता है। गुरु, पूर्णिमा के चांद की तरह, इस अंधेरे में भी रोशनी बिखेरता है। इसलिए, आषाढ़ पूर्णिमा गुरु और शिष्य के मिलन का प्रतीक है, जहां गुरु बादल रूपी शिष्यों के बीच भी चमकता है।
बीसवीं सदी के महानतम संत परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती कहते हैं, “गुरू पूर्णिमा का महत्व गुरू से ज्यादा शिष्य के लिए है। गुरू की तो पूर्णिमा हो गई होती है, तभी वे गुरू होते हैं। पूर्णिमा तो शिष्य की होनी है। तभी गुरू इस मौके पर हमारी आसक्ति की जंजीर को तोड़कर संसार के बंधन से मुक्त कराने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए यह दिन शिष्यों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है।“ सच है कि यदि शिष्य की पूर्णिमा हो जाए तो कई बार गुरू गुर और चेला चीनी वाली कहावत भी चरितार्थ हो जाती है। आदियोगी भगवान शिव से सीधे शिक्षा ग्रहण करने वाले मत्स्येंद्रनाथ जब कामाख्या क्षेत्र में जाकर माया के जाल में फंस गए और भगवान शिव से मिली शिक्षाएं भूल गए थे तो उनके पट्शिष्य गोरखनाथ ने ही उन्हें माया-जाल से मुक्त कराने के लिए लंबा-चौड़ा उपदेश दिया था। परिणाम हुआ कि मत्स्येंद्रनाथ माया से मुक्त होकर पुरानी स्थिति में आ गए थे।
इस तरह, गुरू पूर्णिमा हमें याद दिलाता है कि हमारा प्रारब्ध चाहे जैसा भी हो, यदि हम सद्गुरू के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने को तैयार हैं तो हमारे लिए अस्तित्व का प्रत्येक दरवाजा खुल सकता है। गुरू पूर्णिमा शिष्य-धर्म के निर्वहन का संकल्प लेने का दिन है। रस्मी तौर पर केवल गुरू का गुणगान करने से बात बनने वाली नहीं।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व योग विज्ञान




