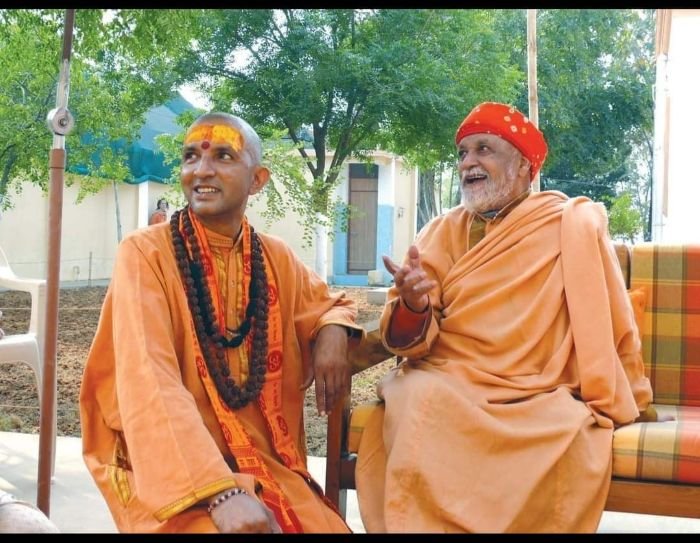इसमें दो मत नहीं कि सद्गुरु की कृपा भगवान की विशेष अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। मनुष्य जब तक संसार के आकर्षणों में रमा रहता है, तब तक उसे अपने भीतर के सत्य की खोज का भाव नहीं जागता। लेकिन जब वह भोगों, आकांक्षाओं और असफलताओं के अनुभवों से थक जाता है, तब धीरे-धीरे उसके भीतर वैराग्य का एक सूक्ष्म बीज अंकुरित होता है।
यह वैराग्य ही आत्मा की जागृति का प्रथम संकेत है। संसार की क्षणभंगुरता जब स्पष्ट होने लगती है, तब मनुष्य की दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है। उसी क्षण ईश्वर की प्रेरणा कार्य करती है, और अपने ही बीच से कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वह सत्संगी हो, साधु हो या साधारण-सा दिखने वाला व्यक्ति, माध्यम बन जाता है। वही सच्चे गुरु के सान्निध्य तक ले जाता है।
यह स्थिति संयोग नहीं होती। यह ईश्वरीय विधान का अंश है, जिसे शास्त्रों और संतों ने प्रमाणित किया है। आदि शंकराचार्य ने विवेकचूडामणि में कहा है – “दुर्लभं त्रयमेवैतत् देवानुग्रहहेतुकम्। मनुष्यत्वं, मुमुक्षुत्वं, महापुरुषसंश्रयः॥” अर्थात्, मनुष्य जन्म, मोक्ष की आकांक्षा और महापुरुष (सद्गुरु) का संग, ये तीनों केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव हैं।
उपनिषदों और योगवासिष्ठ जैसे ग्रंथों में भी यह सिद्धांत बार-बार व्यक्त हुआ है कि जब मनुष्य में वैराग्य जागता है, तभी गुरु की खोज आरंभ होती है और प्रभु की प्रेरणा से वह खोज पूरी होती है। तुलसीदास, मीरा, नरसी मेहता, नामदेव, सभी संतों ने जीवन के क्लेशों से गुजरकर ही गुरु या ईश्वर के साक्षात् अनुभव प्राप्त किए। जब संसार की आशाएँ टूट जाती हैं, तब भीतर का द्वार खुलता है।
इसलिए यह कहा जाता है कि जो सच्चे मन से गुरु को पुकारता है, उसके लिए प्रभु अवश्य कोई न कोई पथ-प्रदर्शक भेज देता है। कई बार यह काम प्रारब्धवश यानी पूर्व जन्मों के सत्कर्मों के कारण भी हो जाता है। गुरु और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं है। गुरु कृपा से प्रभु मिलते हैं, और प्रभु कृपा से गुरु। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक नियम है, जो बार-बार सिद्ध हुआ है।